 कहने को तो हम एक मुक्त समाज हैं, जहाँ हमें बोलने की मुकम्मल आज़ादी है पर यही आज़ादी बहस के नाम पर रोक टोक लगाने के भी काम आ जाती है। फिल्में तो ऐसे मामलों में ज्यादा प्रकाश में आती हैं। कभी आपत्ति फिल्म के टाईटल पर तो कभी एतराज़ कथानक या किरदार पर। आमिर खान की मंगल पांडे को पहले तो खराब प्रेस ज़्यादा मिली फिर फिल्म पिट भी गई। अव्वल तो ऐतिहासिक और पौराणिक पटकथाओं के कद्रदान ही कम होते हैं, तिस पर आज के ज़माने में चीज़ रीमिक्स न की हो तो जंचती नहीं। बहरहाल, आमिर मेहनती अभिनेता हैं, फिल्म के लिये स्वयं को "झोंक" देते हैं (वैसे जिस तरह से वह स्वयं को थोपते हैं, उस लिहाज़ से इस वाक्य में निर्देशक "जोंक देते हैं" जुमले का भी प्रयोग सही मानते), अपने होमवर्क और रीसर्च का गुणगान करते वे थकते नहीं थे। इस बीच बी.बी.सी के एक कर्मी मधुकर उपाध्याय ने १८६० में ब्रितानी सेना के एक सूबेदार सीता राम पाण्डेय की आत्मकथा का अवधी रूपांतर जारी किया है। कहना न होगा कि मौका भी था और दस्तूर भी। अब उपाध्याय का कहना है कि केतन मेहता और आमिर का फिल्म के कथानक की ऐतिहासिक सचाई का दावा बकवास है। कहा कि उन्होंने कोई शोध नहीँ किया, यहाँ तक कि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुरालेखागार में तक नहीं गये जहाँ मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल आर्डर की मूल प्रति संचित है। यानी कुल जमा यह लांक्षन लगा दिया कि फिल्म ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं हैं।
कहने को तो हम एक मुक्त समाज हैं, जहाँ हमें बोलने की मुकम्मल आज़ादी है पर यही आज़ादी बहस के नाम पर रोक टोक लगाने के भी काम आ जाती है। फिल्में तो ऐसे मामलों में ज्यादा प्रकाश में आती हैं। कभी आपत्ति फिल्म के टाईटल पर तो कभी एतराज़ कथानक या किरदार पर। आमिर खान की मंगल पांडे को पहले तो खराब प्रेस ज़्यादा मिली फिर फिल्म पिट भी गई। अव्वल तो ऐतिहासिक और पौराणिक पटकथाओं के कद्रदान ही कम होते हैं, तिस पर आज के ज़माने में चीज़ रीमिक्स न की हो तो जंचती नहीं। बहरहाल, आमिर मेहनती अभिनेता हैं, फिल्म के लिये स्वयं को "झोंक" देते हैं (वैसे जिस तरह से वह स्वयं को थोपते हैं, उस लिहाज़ से इस वाक्य में निर्देशक "जोंक देते हैं" जुमले का भी प्रयोग सही मानते), अपने होमवर्क और रीसर्च का गुणगान करते वे थकते नहीं थे। इस बीच बी.बी.सी के एक कर्मी मधुकर उपाध्याय ने १८६० में ब्रितानी सेना के एक सूबेदार सीता राम पाण्डेय की आत्मकथा का अवधी रूपांतर जारी किया है। कहना न होगा कि मौका भी था और दस्तूर भी। अब उपाध्याय का कहना है कि केतन मेहता और आमिर का फिल्म के कथानक की ऐतिहासिक सचाई का दावा बकवास है। कहा कि उन्होंने कोई शोध नहीँ किया, यहाँ तक कि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुरालेखागार में तक नहीं गये जहाँ मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल आर्डर की मूल प्रति संचित है। यानी कुल जमा यह लांक्षन लगा दिया कि फिल्म ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं हैं।किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाक्रम के नाट्य रूपांतरण में वाकई यह बड़ी दिक्कत है। निर्माता पर वाहवाही व ईनामात बटोरने और बॉक्स आफिस, सब का दबाव रहता है। ओथेंटिसिटी व ऍक्यूरेसी का दावा करना पड़ता है और आलोचक तुरंत जुट जाते हैं दावों में दोष निकालने पर। वैसे न मैंने यह फिल्म देखी है और न ही १८५७ के संग्राम की मेरी जानकारी स्कूली ज्ञान से ज्यादा है, पर मेरा विचार है कि निर्माताओं को अब परिपक्व हो कर ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं में "फिक्शन" या काल्पनिक घटानक्रम का समावेश करने पर उसे स्वीकारने का साहस करना होगा। क्रियेटिव फ्रीडम के आधार पर मुझे यह स्वीकार्य होगा की ऐसी फिल्म बनें जिस में पटकथाकार यह कल्पना करे कि महात्मा गांधी आज जीवित होते तो क्या होता, या फिर कि महाभारत में अर्जुन किसी हालत में भी शस्त्र नहीँ उठाते तो कथानक की दिशा क्या होती। दिक्कत यही है कि निर्माता स्वयं भी परिभाषित नहीं करना चाहते असलियत और कल्पना के दायरे को। जहाँ पौराणिक घटनाओं से अक्सर धार्मिक संवेदनाएँ जुड़ी रहती हैं, तो ऐतिहासिक किरदारों के साथ समुदायों की प्रतिष्ठा और विश्वास का सवाल पैदा हो जाता है। हाँ, ऐतिहासिक घटनाओं के फिल्मीकरण में रिस्क अपेक्षाकृत कम होता है।
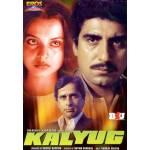 मेरे पसंदीदा निर्देशकों में से एक श्याम बेनेगल की एक फिल्म "कलयुग" में उन्होंने महाभारत को समकालीन सन्दर्भ में बयां किया था, एक फिक्शनल कथा का जामा पहनाकर। पूरी फिल्म में कहीं भी महाकाव्य का हवाला नहीँ दिया, निर्णय दर्शकों पर छोड़ दिया; पात्रों का पौराणिक टेम्पलेट पर चित्रण किया पर हूबहू फॉलो नहीं किया। यह दीगर बात है कि फिल्म उतनी चली नहीं, शायद सन्दर्भ दर्शकों के पल्ले नहीं पड़ा। और शायद इसी बात से फिल्म निर्माता डरते भी हैं। संदेश अगर परोक्ष रूप से, प्रतीकात्मक रूप से दिये जाय, कथानक अगर क्लिष्ट हो तो, फिल्म क्लासेस की बजाय प्रज्ञावान मॉसेस तक सिमट कर रह जाती है। मंगल पांडे फिल्म की कहानी १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम की पृष्ठभूमि में पांडे जैसे सैनिकों के क्रोध से समाज के भीतर बर्तानी हुकुमत और नीतियों के खिलाफ बढ़ते रोष का चित्रण संभव था, पर शायद यह फिर मॉसेस कि फिल्म न रहती, यह किसी कला फिल्म या एब्सट्रैक्ट चित्र जैसा हो जाता, जो चाहे सो मतलब निकाल ले। दूजा सच यह कि आज के ज़माने में हमें हर कथा में सुपरमैन नुमा किरदार चाहिये ही, यह सुपरमैन "डी" के पढ़े लिखे अंडरवर्ल्ड सरगना या "बंटी और बबली" के बंटी हो सकते हैं जो थ्रिल के लिये जुर्म करते है या फिर "सेहेर" का आदर्शवादी एसीपी जो कर्तव्य के लिये जान दे देता है, या फिर डबल्यू.डबल्यू.एफ हूंकार भरता बलवाकारी मंगल। तीजा ये कि, भैया टाईमिंग तो सही रखो, जब "भगत सिंह" टाईप फिल्मों का बाजार गरम था तब आपने ये बनानी शुरु की और फिर तीन चार साल तक बनाते ही रहे और यहाँ ज़माना वाया शाहिद करीना एम.एम.एस "नो एंट्री" तक आ पहुंचा, अब आप परोस रहे हो। हैं भई!
मेरे पसंदीदा निर्देशकों में से एक श्याम बेनेगल की एक फिल्म "कलयुग" में उन्होंने महाभारत को समकालीन सन्दर्भ में बयां किया था, एक फिक्शनल कथा का जामा पहनाकर। पूरी फिल्म में कहीं भी महाकाव्य का हवाला नहीँ दिया, निर्णय दर्शकों पर छोड़ दिया; पात्रों का पौराणिक टेम्पलेट पर चित्रण किया पर हूबहू फॉलो नहीं किया। यह दीगर बात है कि फिल्म उतनी चली नहीं, शायद सन्दर्भ दर्शकों के पल्ले नहीं पड़ा। और शायद इसी बात से फिल्म निर्माता डरते भी हैं। संदेश अगर परोक्ष रूप से, प्रतीकात्मक रूप से दिये जाय, कथानक अगर क्लिष्ट हो तो, फिल्म क्लासेस की बजाय प्रज्ञावान मॉसेस तक सिमट कर रह जाती है। मंगल पांडे फिल्म की कहानी १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम की पृष्ठभूमि में पांडे जैसे सैनिकों के क्रोध से समाज के भीतर बर्तानी हुकुमत और नीतियों के खिलाफ बढ़ते रोष का चित्रण संभव था, पर शायद यह फिर मॉसेस कि फिल्म न रहती, यह किसी कला फिल्म या एब्सट्रैक्ट चित्र जैसा हो जाता, जो चाहे सो मतलब निकाल ले। दूजा सच यह कि आज के ज़माने में हमें हर कथा में सुपरमैन नुमा किरदार चाहिये ही, यह सुपरमैन "डी" के पढ़े लिखे अंडरवर्ल्ड सरगना या "बंटी और बबली" के बंटी हो सकते हैं जो थ्रिल के लिये जुर्म करते है या फिर "सेहेर" का आदर्शवादी एसीपी जो कर्तव्य के लिये जान दे देता है, या फिर डबल्यू.डबल्यू.एफ हूंकार भरता बलवाकारी मंगल। तीजा ये कि, भैया टाईमिंग तो सही रखो, जब "भगत सिंह" टाईप फिल्मों का बाजार गरम था तब आपने ये बनानी शुरु की और फिर तीन चार साल तक बनाते ही रहे और यहाँ ज़माना वाया शाहिद करीना एम.एम.एस "नो एंट्री" तक आ पहुंचा, अब आप परोस रहे हो। हैं भई!वैसे निर्माताओं से ज्यादा दर्शकों पर निर्भर होता है कि दिशा क्या होगी। यहाँ "इकबाल" भी बनती है और "क्या कूल है हम" भी। तो उम्मीद यही की जाय कि प्रयोगधर्मी फिल्मकार ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों को तौल कर लें, पर लें ज़रूर। सच्ची बनाओ या कोरी काल्पनिक, पर बनाओ दिल से। फिर नतीज़ा भले ही डेविड सेल्टज़र लिखित "ओमेन" जैसा बाईबल का सरलीकृत बयान हो या फिर अशोक बैंकर के "रामायण" की तरह यप्पी और टेक्नो, पसंद ज़रूर की जायेगी। आखिरकार बाज़ार में पिज़्ज़ा और नान दोनों की खपत होती है।
1 comment:
बात तो एकदम सोलह आने सही कह रहे हो भइये.
पुरानी बात को आज के संदर्भों में ले के काम करना
चाहिये .हरिशंकर परसाई जी के बहुत सारा लोकप्रिय लेखन पुरानी घटनाओं को फंतासी में लिखने का था.पर अब कोई तुम्हारी सुने तब न!
Post a Comment