घबराईये नहीं नुक्ताचीनी बंद नहीं हुई, बस अब नई जगह होती है !
नुक्ताचीनी का नया पता है http://nuktachini.debashish.com
नुक्ताचीनी की फीड का पाठक बनने हेतु यहाँ क्लिक करें।
Friday, September 30, 2005
नया ब्लॉग वर्गीकरण
क्षेत्रियता और विषय के आधार पर ब्लॉगों के वर्गीकरण तो होते रहते हैं, पहली बार देखा धर्म के नाम पर वर्गीकरण। गॉडब्लॉगकॉन क्रिस्तान ब्लॉगरों का पहला सम्मेलन है जो कथित रूप से इस समुदाय के ब्लॉगरों को एकजुट करेगा। एकजुट ही करना भाया, पृथकता से डर लगता है!
नासा और गूगल
Tuesday, September 27, 2005
पब्लिक सब जानती है
 क्या गांगुली की कप्तानी २००५ के अंत तक टिकेगी? क्या राहुल गांधी २०१० में भारत के प्रधानमंत्री होंगे? ऐसे सवालों के जवाबों की उम्मीद तो अब तक तो हम बेजॉन दारूवाला जैसे लोगों से ही करते थे पर अब ये कयास वैज्ञानिक प्रयासों से काफी सच भी साबित हो सकते हैं। मेरे पसंदीदा चिट्ठाकारों में शामिल नितिन पई और श्रीजीत ने प्रेडिक्शन मार्केट के आर्थिक सिद्धांत पर एक नया प्रयोग किया है, पब्लिक ज्ञान के रूप में। प्रेडिक्शन मार्केट का सिद्धांत कहता है कि अगर ढेर सारे लोगों की व्यक्तिगत राय को सम्मिश्रित कर दिया जाय तो नतीजे वास्तविक नतीजों के काफी करीब होते हैं, जिसका ज़िक्र जेम्स सोरोविकी की कामयाब पुस्तक विस्डम आफ क्राउड में भी है।
क्या गांगुली की कप्तानी २००५ के अंत तक टिकेगी? क्या राहुल गांधी २०१० में भारत के प्रधानमंत्री होंगे? ऐसे सवालों के जवाबों की उम्मीद तो अब तक तो हम बेजॉन दारूवाला जैसे लोगों से ही करते थे पर अब ये कयास वैज्ञानिक प्रयासों से काफी सच भी साबित हो सकते हैं। मेरे पसंदीदा चिट्ठाकारों में शामिल नितिन पई और श्रीजीत ने प्रेडिक्शन मार्केट के आर्थिक सिद्धांत पर एक नया प्रयोग किया है, पब्लिक ज्ञान के रूप में। प्रेडिक्शन मार्केट का सिद्धांत कहता है कि अगर ढेर सारे लोगों की व्यक्तिगत राय को सम्मिश्रित कर दिया जाय तो नतीजे वास्तविक नतीजों के काफी करीब होते हैं, जिसका ज़िक्र जेम्स सोरोविकी की कामयाब पुस्तक विस्डम आफ क्राउड में भी है।पब्लिक ज्ञान में आप अनुमान शेयर बाजार की तईं लगाते हैं फर्क बस इतना है कि खर्च कुछ नहीं करना पड़ता, सारा कारोबार रूपये या डॉलर में नहीं "मूलर" में होता है। मंच पर फिलहाल प्रवेश के लिये निमंत्रण की दरकार होगी। नितिन के इस अभिनव प्रयास के लिये ढेरों शुभकामनायें! स्मार्ट मॉब्स क्या कर सकती हैं यह इसका बेहतरीन उदाहरण बन कर उभरेगा।
टैग: प्रेडिक्शन, मार्केट, पब्लिक, ज्ञान, मूलर, नितिन, पई
आज तन्मय का जन्मदिन
 आज यानि २८ सितंबर २००५ को मेरे पुत्र तन्मय का जन्मदिन है जो अब तीन वर्ष के हो चुके हैं। बेटा तो अभी हैं दादा दादी के पास तो मुझे भी मन मसोस कर फोन पर ही बधाई देनी पड़ेगी।
आज यानि २८ सितंबर २००५ को मेरे पुत्र तन्मय का जन्मदिन है जो अब तीन वर्ष के हो चुके हैं। बेटा तो अभी हैं दादा दादी के पास तो मुझे भी मन मसोस कर फोन पर ही बधाई देनी पड़ेगी।बूबू हम सभी की ओर से तुम्हें हैप्पी बर्थडे और दीर्घ, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिये आशीर्वाद और प्यार। तुम जीयो हज़ारों साल, साल के दिन हो पचास हज़ार!
Monday, September 26, 2005
बोले तो...
- सिक्स अपार्ट २००६ में छोड़ने जा रहा है नया शगूफा, प्रोजेक्ट कॉमेट, जो कहते हैं कि लाईव जर्नल, टाईप पैड और मूवेबल टाईप का सम्मिश्रण है। अब यह कॉमेट कैसा होगा यह तो वो ही जाने पर म्हारे को तो जै याहू ३६० डिग्रीज़ जैसी ही बात लगे है।
- फीड के दीवानों के लिये एक और नया आनलाईन फीडरीडर है फिंडोरी। ब्लॉगलाईंस का सफाया करने को उतारु यह हजरत न केवल कोई भी OPML सूची बल्कि ब्लॉगलाईंस के सब्सक्रिप्शन्स को भी इम्पोर्ट करने का माद्दा रखते हैं। कहा जा रहा कि यह बहुत "तेज़" है, यह बात है तो आज़मा कर देखना पड़ेगा!
- नाम कमाना है तो जर्मनी के देशवैले द्वारा आयोजित ब्लॉग अवार्ड में शुमार हों। बताना तो वैबी अवार्ड के बारे में भी चाहता हूँ पर यहाँ तो कुछ जीतने के लिये दमड़ी लगेगी। दूर से प्रणाम!
Sunday, September 11, 2005
अब तो छोड़ो मोह!
हाल ही में हास्य कवि प्रदीप चौबे के दो लाईना पर पुनः नज़र पड़ीः
सत्ता को लालायित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बारे में यह काफी सटीक वचन हैं। सत्ता से विछोह के बाद से उपरी तौर पर सुगठित दिखने वाले संगठन की अंदरूनी दरारें तो खैर काफी दिनों से नज़र आ ही रही थीं। सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, उमा भारती जैसे अनेकों टकटकी लगाये बैठे रहे हैं की पार्टी में उनका कुछ दबदबा कायम हो। राजनीति के पानी की सचाई यही है कि जो नेता मुखरित रूप से सतह पर नज़र आते हैं उनका वज़न वैज्ञानिक नियमों के तहत हल्का ही होता है। जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़ने के बाद से ही आडवाणी का सिंहासन डोल उठा था, खुराना जैसे लोग इस फ़िराक में थे कि इसी तेज़ कैटरियानी बयार की ओट में अपना उल्लू सीधा हो जाय तो अच्छा। खुराना और उमा जैसे नेताओं का पार्टी में आधार ठीकठाक है पर समय समय पर पार्टी इनसे कर्त्तव्य पालन के नाम पर बलिदान भी मांगती रही है, उमा को मध्यप्रदेश का ताज़ सौंपना पड़ा गौर को तो खुराना भी हाशिये पर आने को मजबूर हुए। कल वाजपेयी और आडवाणी के मनमुटाव का फायदा ले कर बचने की सोच रहे खुराना के राजनैतिक करियर की ताबूत में आखिरकार अंतिम कील जड़ ही दी गई, हालांकि काँग्रेस शायद जल्द ही प्राणवायु पुनः फूंकने का प्रयास करे। खुराना के खुर कतरने के पीछे पार्टी का साफ संकेत यहः की पंगा ना लै मेरे नाल।
वाजपेयी के हालिया राजनैतिक चुप्पी से उपजते मोहभंग के शब्द से मेरा यह विचार बना था कि चलो शायद भाजपा इस बारे में राजनैतिक अपवाद बने और शीर्ष नेता ससम्मान पदत्याग कर नये लोगों को, खास तौर पर पुराने मोहरों को, आगे आने का मौका दें। पार्टी की सेहत की ज़मीन के लिये भी यह गुड़ाई अच्छी होती, नीचे की उपजाउ ज़मीन उपर आती और खरपतवार भी साफ होते। पर परिणाम में फिर वही ढाक के तीन पात! फिर वही पॉवर स्ट्रगल, वही पुरानी लड़ाई वर्चस्व की। अरे भैये, ८५-९० पार कर लिये आपने, जाने कब बुलावा आ जाय, जितनी इज़्जत और पैसा बनाना था सो तो बना ही लिया होगा, अब तो छोड़ो मोह। पद पर रह कर भी क्या रहे हो? क्या अगले चुनाव की ज़मीनी तैयारी है? क्या सहयोगी दल से अभी भी यारी है? इन दलों की छोड़ो, क्या संघ और शिव सेना अब भी मन के मीत हैं? क्या संगठन की मजबूती भीत है? हर रोज़ तो आप लोग बयान बदलते हो, दोनों शीर्ष नेताओं में ही नहीं पट रही। फिर काहे के बड़े हो? सचाई का सामना करो, उम्र का लिहाज़ करो, सचमुच बड़ा बने रहना है तो बड़ा निर्णय तो लेना ही होगा।
काहे के बड़े हैं,
अगर दही में पड़े हैं।
सत्ता को लालायित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बारे में यह काफी सटीक वचन हैं। सत्ता से विछोह के बाद से उपरी तौर पर सुगठित दिखने वाले संगठन की अंदरूनी दरारें तो खैर काफी दिनों से नज़र आ ही रही थीं। सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, उमा भारती जैसे अनेकों टकटकी लगाये बैठे रहे हैं की पार्टी में उनका कुछ दबदबा कायम हो। राजनीति के पानी की सचाई यही है कि जो नेता मुखरित रूप से सतह पर नज़र आते हैं उनका वज़न वैज्ञानिक नियमों के तहत हल्का ही होता है। जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़ने के बाद से ही आडवाणी का सिंहासन डोल उठा था, खुराना जैसे लोग इस फ़िराक में थे कि इसी तेज़ कैटरियानी बयार की ओट में अपना उल्लू सीधा हो जाय तो अच्छा। खुराना और उमा जैसे नेताओं का पार्टी में आधार ठीकठाक है पर समय समय पर पार्टी इनसे कर्त्तव्य पालन के नाम पर बलिदान भी मांगती रही है, उमा को मध्यप्रदेश का ताज़ सौंपना पड़ा गौर को तो खुराना भी हाशिये पर आने को मजबूर हुए। कल वाजपेयी और आडवाणी के मनमुटाव का फायदा ले कर बचने की सोच रहे खुराना के राजनैतिक करियर की ताबूत में आखिरकार अंतिम कील जड़ ही दी गई, हालांकि काँग्रेस शायद जल्द ही प्राणवायु पुनः फूंकने का प्रयास करे। खुराना के खुर कतरने के पीछे पार्टी का साफ संकेत यहः की पंगा ना लै मेरे नाल।
वाजपेयी के हालिया राजनैतिक चुप्पी से उपजते मोहभंग के शब्द से मेरा यह विचार बना था कि चलो शायद भाजपा इस बारे में राजनैतिक अपवाद बने और शीर्ष नेता ससम्मान पदत्याग कर नये लोगों को, खास तौर पर पुराने मोहरों को, आगे आने का मौका दें। पार्टी की सेहत की ज़मीन के लिये भी यह गुड़ाई अच्छी होती, नीचे की उपजाउ ज़मीन उपर आती और खरपतवार भी साफ होते। पर परिणाम में फिर वही ढाक के तीन पात! फिर वही पॉवर स्ट्रगल, वही पुरानी लड़ाई वर्चस्व की। अरे भैये, ८५-९० पार कर लिये आपने, जाने कब बुलावा आ जाय, जितनी इज़्जत और पैसा बनाना था सो तो बना ही लिया होगा, अब तो छोड़ो मोह। पद पर रह कर भी क्या रहे हो? क्या अगले चुनाव की ज़मीनी तैयारी है? क्या सहयोगी दल से अभी भी यारी है? इन दलों की छोड़ो, क्या संघ और शिव सेना अब भी मन के मीत हैं? क्या संगठन की मजबूती भीत है? हर रोज़ तो आप लोग बयान बदलते हो, दोनों शीर्ष नेताओं में ही नहीं पट रही। फिर काहे के बड़े हो? सचाई का सामना करो, उम्र का लिहाज़ करो, सचमुच बड़ा बने रहना है तो बड़ा निर्णय तो लेना ही होगा।
Thursday, September 08, 2005
मंगल पर दंगल
 कहने को तो हम एक मुक्त समाज हैं, जहाँ हमें बोलने की मुकम्मल आज़ादी है पर यही आज़ादी बहस के नाम पर रोक टोक लगाने के भी काम आ जाती है। फिल्में तो ऐसे मामलों में ज्यादा प्रकाश में आती हैं। कभी आपत्ति फिल्म के टाईटल पर तो कभी एतराज़ कथानक या किरदार पर। आमिर खान की मंगल पांडे को पहले तो खराब प्रेस ज़्यादा मिली फिर फिल्म पिट भी गई। अव्वल तो ऐतिहासिक और पौराणिक पटकथाओं के कद्रदान ही कम होते हैं, तिस पर आज के ज़माने में चीज़ रीमिक्स न की हो तो जंचती नहीं। बहरहाल, आमिर मेहनती अभिनेता हैं, फिल्म के लिये स्वयं को "झोंक" देते हैं (वैसे जिस तरह से वह स्वयं को थोपते हैं, उस लिहाज़ से इस वाक्य में निर्देशक "जोंक देते हैं" जुमले का भी प्रयोग सही मानते), अपने होमवर्क और रीसर्च का गुणगान करते वे थकते नहीं थे। इस बीच बी.बी.सी के एक कर्मी मधुकर उपाध्याय ने १८६० में ब्रितानी सेना के एक सूबेदार सीता राम पाण्डेय की आत्मकथा का अवधी रूपांतर जारी किया है। कहना न होगा कि मौका भी था और दस्तूर भी। अब उपाध्याय का कहना है कि केतन मेहता और आमिर का फिल्म के कथानक की ऐतिहासिक सचाई का दावा बकवास है। कहा कि उन्होंने कोई शोध नहीँ किया, यहाँ तक कि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुरालेखागार में तक नहीं गये जहाँ मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल आर्डर की मूल प्रति संचित है। यानी कुल जमा यह लांक्षन लगा दिया कि फिल्म ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं हैं।
कहने को तो हम एक मुक्त समाज हैं, जहाँ हमें बोलने की मुकम्मल आज़ादी है पर यही आज़ादी बहस के नाम पर रोक टोक लगाने के भी काम आ जाती है। फिल्में तो ऐसे मामलों में ज्यादा प्रकाश में आती हैं। कभी आपत्ति फिल्म के टाईटल पर तो कभी एतराज़ कथानक या किरदार पर। आमिर खान की मंगल पांडे को पहले तो खराब प्रेस ज़्यादा मिली फिर फिल्म पिट भी गई। अव्वल तो ऐतिहासिक और पौराणिक पटकथाओं के कद्रदान ही कम होते हैं, तिस पर आज के ज़माने में चीज़ रीमिक्स न की हो तो जंचती नहीं। बहरहाल, आमिर मेहनती अभिनेता हैं, फिल्म के लिये स्वयं को "झोंक" देते हैं (वैसे जिस तरह से वह स्वयं को थोपते हैं, उस लिहाज़ से इस वाक्य में निर्देशक "जोंक देते हैं" जुमले का भी प्रयोग सही मानते), अपने होमवर्क और रीसर्च का गुणगान करते वे थकते नहीं थे। इस बीच बी.बी.सी के एक कर्मी मधुकर उपाध्याय ने १८६० में ब्रितानी सेना के एक सूबेदार सीता राम पाण्डेय की आत्मकथा का अवधी रूपांतर जारी किया है। कहना न होगा कि मौका भी था और दस्तूर भी। अब उपाध्याय का कहना है कि केतन मेहता और आमिर का फिल्म के कथानक की ऐतिहासिक सचाई का दावा बकवास है। कहा कि उन्होंने कोई शोध नहीँ किया, यहाँ तक कि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुरालेखागार में तक नहीं गये जहाँ मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल आर्डर की मूल प्रति संचित है। यानी कुल जमा यह लांक्षन लगा दिया कि फिल्म ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं हैं।किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाक्रम के नाट्य रूपांतरण में वाकई यह बड़ी दिक्कत है। निर्माता पर वाहवाही व ईनामात बटोरने और बॉक्स आफिस, सब का दबाव रहता है। ओथेंटिसिटी व ऍक्यूरेसी का दावा करना पड़ता है और आलोचक तुरंत जुट जाते हैं दावों में दोष निकालने पर। वैसे न मैंने यह फिल्म देखी है और न ही १८५७ के संग्राम की मेरी जानकारी स्कूली ज्ञान से ज्यादा है, पर मेरा विचार है कि निर्माताओं को अब परिपक्व हो कर ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं में "फिक्शन" या काल्पनिक घटानक्रम का समावेश करने पर उसे स्वीकारने का साहस करना होगा। क्रियेटिव फ्रीडम के आधार पर मुझे यह स्वीकार्य होगा की ऐसी फिल्म बनें जिस में पटकथाकार यह कल्पना करे कि महात्मा गांधी आज जीवित होते तो क्या होता, या फिर कि महाभारत में अर्जुन किसी हालत में भी शस्त्र नहीँ उठाते तो कथानक की दिशा क्या होती। दिक्कत यही है कि निर्माता स्वयं भी परिभाषित नहीं करना चाहते असलियत और कल्पना के दायरे को। जहाँ पौराणिक घटनाओं से अक्सर धार्मिक संवेदनाएँ जुड़ी रहती हैं, तो ऐतिहासिक किरदारों के साथ समुदायों की प्रतिष्ठा और विश्वास का सवाल पैदा हो जाता है। हाँ, ऐतिहासिक घटनाओं के फिल्मीकरण में रिस्क अपेक्षाकृत कम होता है।
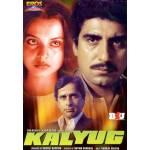 मेरे पसंदीदा निर्देशकों में से एक श्याम बेनेगल की एक फिल्म "कलयुग" में उन्होंने महाभारत को समकालीन सन्दर्भ में बयां किया था, एक फिक्शनल कथा का जामा पहनाकर। पूरी फिल्म में कहीं भी महाकाव्य का हवाला नहीँ दिया, निर्णय दर्शकों पर छोड़ दिया; पात्रों का पौराणिक टेम्पलेट पर चित्रण किया पर हूबहू फॉलो नहीं किया। यह दीगर बात है कि फिल्म उतनी चली नहीं, शायद सन्दर्भ दर्शकों के पल्ले नहीं पड़ा। और शायद इसी बात से फिल्म निर्माता डरते भी हैं। संदेश अगर परोक्ष रूप से, प्रतीकात्मक रूप से दिये जाय, कथानक अगर क्लिष्ट हो तो, फिल्म क्लासेस की बजाय प्रज्ञावान मॉसेस तक सिमट कर रह जाती है। मंगल पांडे फिल्म की कहानी १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम की पृष्ठभूमि में पांडे जैसे सैनिकों के क्रोध से समाज के भीतर बर्तानी हुकुमत और नीतियों के खिलाफ बढ़ते रोष का चित्रण संभव था, पर शायद यह फिर मॉसेस कि फिल्म न रहती, यह किसी कला फिल्म या एब्सट्रैक्ट चित्र जैसा हो जाता, जो चाहे सो मतलब निकाल ले। दूजा सच यह कि आज के ज़माने में हमें हर कथा में सुपरमैन नुमा किरदार चाहिये ही, यह सुपरमैन "डी" के पढ़े लिखे अंडरवर्ल्ड सरगना या "बंटी और बबली" के बंटी हो सकते हैं जो थ्रिल के लिये जुर्म करते है या फिर "सेहेर" का आदर्शवादी एसीपी जो कर्तव्य के लिये जान दे देता है, या फिर डबल्यू.डबल्यू.एफ हूंकार भरता बलवाकारी मंगल। तीजा ये कि, भैया टाईमिंग तो सही रखो, जब "भगत सिंह" टाईप फिल्मों का बाजार गरम था तब आपने ये बनानी शुरु की और फिर तीन चार साल तक बनाते ही रहे और यहाँ ज़माना वाया शाहिद करीना एम.एम.एस "नो एंट्री" तक आ पहुंचा, अब आप परोस रहे हो। हैं भई!
मेरे पसंदीदा निर्देशकों में से एक श्याम बेनेगल की एक फिल्म "कलयुग" में उन्होंने महाभारत को समकालीन सन्दर्भ में बयां किया था, एक फिक्शनल कथा का जामा पहनाकर। पूरी फिल्म में कहीं भी महाकाव्य का हवाला नहीँ दिया, निर्णय दर्शकों पर छोड़ दिया; पात्रों का पौराणिक टेम्पलेट पर चित्रण किया पर हूबहू फॉलो नहीं किया। यह दीगर बात है कि फिल्म उतनी चली नहीं, शायद सन्दर्भ दर्शकों के पल्ले नहीं पड़ा। और शायद इसी बात से फिल्म निर्माता डरते भी हैं। संदेश अगर परोक्ष रूप से, प्रतीकात्मक रूप से दिये जाय, कथानक अगर क्लिष्ट हो तो, फिल्म क्लासेस की बजाय प्रज्ञावान मॉसेस तक सिमट कर रह जाती है। मंगल पांडे फिल्म की कहानी १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम की पृष्ठभूमि में पांडे जैसे सैनिकों के क्रोध से समाज के भीतर बर्तानी हुकुमत और नीतियों के खिलाफ बढ़ते रोष का चित्रण संभव था, पर शायद यह फिर मॉसेस कि फिल्म न रहती, यह किसी कला फिल्म या एब्सट्रैक्ट चित्र जैसा हो जाता, जो चाहे सो मतलब निकाल ले। दूजा सच यह कि आज के ज़माने में हमें हर कथा में सुपरमैन नुमा किरदार चाहिये ही, यह सुपरमैन "डी" के पढ़े लिखे अंडरवर्ल्ड सरगना या "बंटी और बबली" के बंटी हो सकते हैं जो थ्रिल के लिये जुर्म करते है या फिर "सेहेर" का आदर्शवादी एसीपी जो कर्तव्य के लिये जान दे देता है, या फिर डबल्यू.डबल्यू.एफ हूंकार भरता बलवाकारी मंगल। तीजा ये कि, भैया टाईमिंग तो सही रखो, जब "भगत सिंह" टाईप फिल्मों का बाजार गरम था तब आपने ये बनानी शुरु की और फिर तीन चार साल तक बनाते ही रहे और यहाँ ज़माना वाया शाहिद करीना एम.एम.एस "नो एंट्री" तक आ पहुंचा, अब आप परोस रहे हो। हैं भई!वैसे निर्माताओं से ज्यादा दर्शकों पर निर्भर होता है कि दिशा क्या होगी। यहाँ "इकबाल" भी बनती है और "क्या कूल है हम" भी। तो उम्मीद यही की जाय कि प्रयोगधर्मी फिल्मकार ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों को तौल कर लें, पर लें ज़रूर। सच्ची बनाओ या कोरी काल्पनिक, पर बनाओ दिल से। फिर नतीज़ा भले ही डेविड सेल्टज़र लिखित "ओमेन" जैसा बाईबल का सरलीकृत बयान हो या फिर अशोक बैंकर के "रामायण" की तरह यप्पी और टेक्नो, पसंद ज़रूर की जायेगी। आखिरकार बाज़ार में पिज़्ज़ा और नान दोनों की खपत होती है।
Sunday, September 04, 2005
अब अबला कहाँ?
फिल्म माई वाईफ्स मर्डर में अनिल कपूर के निभाये पात्र के हाथों अपनी पत्नी का कत्ल हो जाता है। यह फिल्म वैसे किसी चर्चा के लायक नहीं हैं, पर स्टार के ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में व्यंग्य किया गया कि जहाँ महिलायें कथानक में गुस्सेल पति के बड़ी आसानी से छूट जाने पर खफा हैं तो पतियों को "एक्सीडेंट" के आईडिया मिल रहे हैं। कथानकों में आम तौर पर पति का निर्दोष पक्ष यदा कदा ही दिखता है। यह एक विचित्र सत्य भी है कि हमारे लतीफों में नारी बेलनधारी खलनायिका तो साहित्य में पीड़ित नायिका के रूप में चित्रित होती रही हैं। इन दोनों पक्षों में पुरुष का चित्रण दयनीय ही रहता है। अब मुझे नारी विरोधी या मेल शॉवीनिज़्म के आरोपों से अलंकृत न किया जाय तो मैं यह कहुँगा कि कम से कम आज के युग में छुइमुइ, निरीह और भारतीय संस्कारों के बुरके में कैद नारी की छवि अपने मन में चित्रित करना मुश्किल ही होता जा रहा है। ज़माना बदल गया है और स्त्री हर पल यह जता भी रही हैं। सिनेमा और टीवी के पर्दों पर कंधा न सही अन्य सारे अंग पुरुषों के साथ मिला कर आगे बढ़ रही हैं। मुम्बई व पुणे आने के बाद मैंने देखा कि दरअसल जो सिनेमा में दिख रहा है वो समाज का अक्स ही है, सिर्फ अंतर्वस्त्र दर्शना जीन्स (मराठी में जिसे मज़ाक में ABCD यानि "अगो बाइ चड्डी दिसते" भी कहते हैं) ही नहीं आर्दश भी हैं आल टाईम लो। पुणे यूनिवर्सिटी हो या सिम्बी, देर रात तक काममोहित जोड़ों को मंडराते देखना आम बात है। मेरे एक मित्र ने कहा कि पुणे मुम्बई में ज्यादा सुरक्षा होने का कॉलेज षोडषियां अब नाजायज फायदा उठा रही हैं।
 बहरहाल, अबला नारी का जो तमगा साहित्य में जड़ा जा चुका है वह शहरी क्षेत्र में किसी भी हालत में लागू नहीं हो सकता। यहां की नार गाड़ियाँ ही नहीं हर जगह "स्पीड" की ख्वाहिशमंद हैं। नौकरियों ने उन्हें जरूरी आत्मविश्वास भी दिया है। जो नौकरी न भी करती हों पर जिनके मम्मी पापा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है उनके पतियों को भी यह बात भूलने नहीं दी जाती। दरवाज़े पर नेमप्लेट से लेकर, मेडेन सरनेम रखने की जिद तक। "माई वाईफ्स मर्डर" में बोमन ईरानी के निभाये ईंस्पेक्टर के किरदार को उसकी पत्नी यह भूलने नहीं देती कि उसकी पदौन्नति "पापा" की कृपा है। आज लक्ष्मण का कार्टून (देखें चित्र) देखा तो फिल्म का यह अंश याद आ गया। तो भैया अगली दफा किसी शहरी अबला नारी के संतापों की कहानी देखने पढ़ने के पहले हम नमकदानी साथ ज़रूर रखेंगे।
बहरहाल, अबला नारी का जो तमगा साहित्य में जड़ा जा चुका है वह शहरी क्षेत्र में किसी भी हालत में लागू नहीं हो सकता। यहां की नार गाड़ियाँ ही नहीं हर जगह "स्पीड" की ख्वाहिशमंद हैं। नौकरियों ने उन्हें जरूरी आत्मविश्वास भी दिया है। जो नौकरी न भी करती हों पर जिनके मम्मी पापा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है उनके पतियों को भी यह बात भूलने नहीं दी जाती। दरवाज़े पर नेमप्लेट से लेकर, मेडेन सरनेम रखने की जिद तक। "माई वाईफ्स मर्डर" में बोमन ईरानी के निभाये ईंस्पेक्टर के किरदार को उसकी पत्नी यह भूलने नहीं देती कि उसकी पदौन्नति "पापा" की कृपा है। आज लक्ष्मण का कार्टून (देखें चित्र) देखा तो फिल्म का यह अंश याद आ गया। तो भैया अगली दफा किसी शहरी अबला नारी के संतापों की कहानी देखने पढ़ने के पहले हम नमकदानी साथ ज़रूर रखेंगे।
 बहरहाल, अबला नारी का जो तमगा साहित्य में जड़ा जा चुका है वह शहरी क्षेत्र में किसी भी हालत में लागू नहीं हो सकता। यहां की नार गाड़ियाँ ही नहीं हर जगह "स्पीड" की ख्वाहिशमंद हैं। नौकरियों ने उन्हें जरूरी आत्मविश्वास भी दिया है। जो नौकरी न भी करती हों पर जिनके मम्मी पापा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है उनके पतियों को भी यह बात भूलने नहीं दी जाती। दरवाज़े पर नेमप्लेट से लेकर, मेडेन सरनेम रखने की जिद तक। "माई वाईफ्स मर्डर" में बोमन ईरानी के निभाये ईंस्पेक्टर के किरदार को उसकी पत्नी यह भूलने नहीं देती कि उसकी पदौन्नति "पापा" की कृपा है। आज लक्ष्मण का कार्टून (देखें चित्र) देखा तो फिल्म का यह अंश याद आ गया। तो भैया अगली दफा किसी शहरी अबला नारी के संतापों की कहानी देखने पढ़ने के पहले हम नमकदानी साथ ज़रूर रखेंगे।
बहरहाल, अबला नारी का जो तमगा साहित्य में जड़ा जा चुका है वह शहरी क्षेत्र में किसी भी हालत में लागू नहीं हो सकता। यहां की नार गाड़ियाँ ही नहीं हर जगह "स्पीड" की ख्वाहिशमंद हैं। नौकरियों ने उन्हें जरूरी आत्मविश्वास भी दिया है। जो नौकरी न भी करती हों पर जिनके मम्मी पापा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है उनके पतियों को भी यह बात भूलने नहीं दी जाती। दरवाज़े पर नेमप्लेट से लेकर, मेडेन सरनेम रखने की जिद तक। "माई वाईफ्स मर्डर" में बोमन ईरानी के निभाये ईंस्पेक्टर के किरदार को उसकी पत्नी यह भूलने नहीं देती कि उसकी पदौन्नति "पापा" की कृपा है। आज लक्ष्मण का कार्टून (देखें चित्र) देखा तो फिल्म का यह अंश याद आ गया। तो भैया अगली दफा किसी शहरी अबला नारी के संतापों की कहानी देखने पढ़ने के पहले हम नमकदानी साथ ज़रूर रखेंगे।