फिल्में क्यों देखता हूँ? मुझे अच्छा लगता है। हम सभी आक्सीजन, जल और हवा पर जीते हैं पर मन की खुराक कुछ और ही होती है। फिल्में मुझे भाती हैं। जब कभी मन खराब होता है तो यह मुझे गुदगुदाकर हंसा देती है, जब अकेला होता हूँ तो मेरा साथ देती हैं, जब परिवार और मित्र साथ होते हैं तो बढ़िया दोस्त बन जाती है। आजकल तो खैर सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखना मुश्किल होता है तो टीवी या कंप्यूटर ही माध्यम बने हैं सिनेमा दर्शन के। मैंने अक्सर यह सोचा है कि मुझे किस तरह की फिल्में पसंद हैं पर सचाई यही लगती है कि स्थितिजन्य कारणों से कोई फिल्म पसंद आती है और कोई नहीं, कई बार उद्देश्यपूर्ण सिनेमा पसंद आ जाता है तो कई बार बेसिरपैर का धमाल भा जाता है। शायद इसीलिये सलाम नमस्ते पसंद आई पर जेम्स नहीं, सत्या अच्छी लगी पर सेहर नहीं।
फिल्मों के अलावा मुझे फिल्म निर्माण की तकनीक में भी खासी रुचि रहती है, शायद यह बहुत लोगों को पसंद होता है शायद इसीलिये "बिहाईंड द सीन्स" कार्यक्रमों की भरमार है छोटे पर्दे पर। पहले जैकी चैन की फिल्मों के "एंड क्रेडिट्स" के पहले "गूफ अप्स" और खतरनाक शॉट्स के नज़ारों का इंतज़ार रहता था आजकल तो तकरीबन हर फिल्म में यह करने का रिवाज़ हो गया है। बहुत पहले मुम्बई दूरदर्शन से एक कार्यक्रम आता था, "बातें फिल्मों की" जिसे बेंजामिन गिलानी प्रस्तुत करते थे, यह फिल्म निर्माण विधा पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, तब मैं छोटा था पर मुझे यही लगता था की मैं बड़ा होकर फिल्म निर्माण ज़रूर करूंगा, बाबा ने एक मिनी प्रोजेक्टर भी ला दिया था, फिल्मों के टुकड़ों को माँ की साड़ी तब तक दिखाना जब तक की ब्लब वाला टीन का डिब्बा इतना गर्म न हो जाय जब तक की जलने की बू आने लगे। गणेशोत्सव के समय मुहल्ले के सबसे बड़े मैदान पर फिल्म दिखाई जाती तो बड़ा मज़ा आता, चादर बिछा कर प्रोजे्क्टर के सबसे नज़दीक बैठने की होड़ होती, उससे निकलते प्रकाश के रेले में तैरते कणों पर ही नज़र टिकी रहती, और जब गर्मी कई बार रील पिघलकर टूट जाती तो ऐसा लगता की परदे पर किसी ने मर्तबान भर शहद फेंक दिया हो, तब अपना मिनी प्रोजेक्टर याद आ जाता।
फिल्मों में जो चीज़ भाती है वह संगीत भी है। फिल्मी संगीत तो खैर भारतियों की रुह में बसती है। आजकल संगीत फिल्म के काफी पहले जारी हो जाता है, फिर चैनलों पर लगातार बजते बजते हिट भी घोषित हो जाता है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि कर्णप्रिय संगीत अक्सर सुनने को मिल जाता है, हीमेश रेशमिया, प्रीतम जैसे नये लोग नये संगीत के साथ मकबूल हो रहे हैं। आजकल की फिल्मों में हॉलीवुड की नकल की बजाय उसकी तर्ज पर चलने का माहौल गर्माया है, "एक अजनबी" जैसी फिल्मों के साथ हॉलिवुड के कथित निर्देशक भी मैदान में हैं। इससे अब्बास मस्तान, विक्रम भट्ट और संजय गुप्ता जैसे निर्देशकों को, जो या हॉलिवुड की फिल्मों से सीधे "इंस्पायर" हो जाते रहे हैं को सबक मिलेगा। हमें हॉलीवुड जैसी प्रोफेशनलिज़्म और प्रबंधन तथा तकनीकी कौशल को अपनाने की ज्यादा ज़रूरत है बनिस्बत की इनकी पटकथाओं का अनुसरण करने की। फिल्में जल्दी बनें, पेशेवराना रूप से बने, तो लागत भी घटे।
फिल्में मुझे हर रूप में पसंद आती हैं, चाहे फंतासी हो या यथार्थ के नज़दीक। आजकल की फिल्मों में खास यह बात अच्छी लगती है कि तकनीक बढ़िया हुई है और अदाकारी से भी हैम और मेलोड्रामा का अंश लगभग खत्म हो गया है। सुना है की भारतीय कंपनियाँ एनीमेशन और स्पेशल अफेक्ट्स में हॉलिवुड से काम पा रही हैं। मुझे इंतज़ार उस दिन का रहेगा जब हम जूरासिक पार्क जैसी कोई करिश्माई फिल्म मूल पटकथा और अपने माद्दे पर बनायेंगे, जिसे आस्कर में किसी से होड़ नहीं करनी होगी।



 कहने को तो हम एक मुक्त समाज हैं, जहाँ हमें बोलने की मुकम्मल आज़ादी है पर यही आज़ादी बहस के नाम पर रोक टोक लगाने के भी काम आ जाती है। फिल्में तो ऐसे मामलों में ज्यादा प्रकाश में आती हैं। कभी आपत्ति फिल्म के टाईटल पर तो कभी एतराज़ कथानक या किरदार पर। आमिर खान की
कहने को तो हम एक मुक्त समाज हैं, जहाँ हमें बोलने की मुकम्मल आज़ादी है पर यही आज़ादी बहस के नाम पर रोक टोक लगाने के भी काम आ जाती है। फिल्में तो ऐसे मामलों में ज्यादा प्रकाश में आती हैं। कभी आपत्ति फिल्म के टाईटल पर तो कभी एतराज़ कथानक या किरदार पर। आमिर खान की 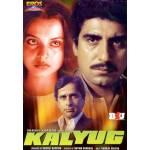 मेरे पसंदीदा निर्देशकों में से एक श्याम बेनेगल की एक फिल्म "कलयुग" में उन्होंने महाभारत को समकालीन सन्दर्भ में बयां किया था, एक फिक्शनल कथा का जामा पहनाकर। पूरी फिल्म में कहीं भी महाकाव्य का हवाला नहीँ दिया, निर्णय दर्शकों पर छोड़ दिया; पात्रों का पौराणिक टेम्पलेट पर चित्रण किया पर हूबहू फॉलो नहीं किया। यह दीगर बात है कि फिल्म उतनी चली नहीं, शायद सन्दर्भ दर्शकों के पल्ले नहीं पड़ा। और शायद इसी बात से फिल्म निर्माता डरते भी हैं। संदेश अगर परोक्ष रूप से, प्रतीकात्मक रूप से दिये जाय, कथानक अगर क्लिष्ट हो तो, फिल्म क्लासेस की बजाय प्रज्ञावान मॉसेस तक सिमट कर रह जाती है। मंगल पांडे फिल्म की कहानी १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम की पृष्ठभूमि में पांडे जैसे सैनिकों के क्रोध से समाज के भीतर बर्तानी हुकुमत और नीतियों के खिलाफ बढ़ते रोष का चित्रण संभव था, पर शायद यह फिर मॉसेस कि फिल्म न रहती, यह किसी कला फिल्म या एब्सट्रैक्ट चित्र जैसा हो जाता, जो चाहे सो मतलब निकाल ले। दूजा सच यह कि आज के ज़माने में हमें हर कथा में सुपरमैन नुमा किरदार चाहिये ही, यह सुपरमैन "डी" के पढ़े लिखे अंडरवर्ल्ड सरगना या "बंटी और बबली" के बंटी हो सकते हैं जो थ्रिल के लिये जुर्म करते है या फिर "सेहेर" का आदर्शवादी एसीपी जो कर्तव्य के लिये जान दे देता है, या फिर डबल्यू.डबल्यू.एफ हूंकार भरता बलवाकारी मंगल। तीजा ये कि, भैया टाईमिंग तो सही रखो, जब "भगत सिंह" टाईप फिल्मों का बाजार गरम था तब आपने ये बनानी शुरु की और फिर तीन चार साल तक बनाते ही रहे और यहाँ ज़माना वाया शाहिद करीना एम.एम.एस "नो एंट्री" तक आ पहुंचा, अब आप परोस रहे हो। हैं भई!
मेरे पसंदीदा निर्देशकों में से एक श्याम बेनेगल की एक फिल्म "कलयुग" में उन्होंने महाभारत को समकालीन सन्दर्भ में बयां किया था, एक फिक्शनल कथा का जामा पहनाकर। पूरी फिल्म में कहीं भी महाकाव्य का हवाला नहीँ दिया, निर्णय दर्शकों पर छोड़ दिया; पात्रों का पौराणिक टेम्पलेट पर चित्रण किया पर हूबहू फॉलो नहीं किया। यह दीगर बात है कि फिल्म उतनी चली नहीं, शायद सन्दर्भ दर्शकों के पल्ले नहीं पड़ा। और शायद इसी बात से फिल्म निर्माता डरते भी हैं। संदेश अगर परोक्ष रूप से, प्रतीकात्मक रूप से दिये जाय, कथानक अगर क्लिष्ट हो तो, फिल्म क्लासेस की बजाय प्रज्ञावान मॉसेस तक सिमट कर रह जाती है। मंगल पांडे फिल्म की कहानी १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम की पृष्ठभूमि में पांडे जैसे सैनिकों के क्रोध से समाज के भीतर बर्तानी हुकुमत और नीतियों के खिलाफ बढ़ते रोष का चित्रण संभव था, पर शायद यह फिर मॉसेस कि फिल्म न रहती, यह किसी कला फिल्म या एब्सट्रैक्ट चित्र जैसा हो जाता, जो चाहे सो मतलब निकाल ले। दूजा सच यह कि आज के ज़माने में हमें हर कथा में सुपरमैन नुमा किरदार चाहिये ही, यह सुपरमैन "डी" के पढ़े लिखे अंडरवर्ल्ड सरगना या "बंटी और बबली" के बंटी हो सकते हैं जो थ्रिल के लिये जुर्म करते है या फिर "सेहेर" का आदर्शवादी एसीपी जो कर्तव्य के लिये जान दे देता है, या फिर डबल्यू.डबल्यू.एफ हूंकार भरता बलवाकारी मंगल। तीजा ये कि, भैया टाईमिंग तो सही रखो, जब "भगत सिंह" टाईप फिल्मों का बाजार गरम था तब आपने ये बनानी शुरु की और फिर तीन चार साल तक बनाते ही रहे और यहाँ ज़माना वाया शाहिद करीना एम.एम.एस "नो एंट्री" तक आ पहुंचा, अब आप परोस रहे हो। हैं भई!